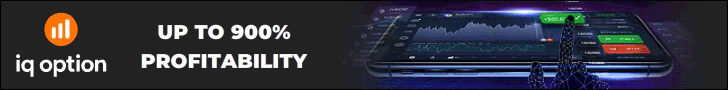जलवायु समझौता
- जलवायु समझौता: एक विस्तृत विश्लेषण
जलवायु समझौता एक ऐसा शब्द है जो हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर तेजी से महत्वपूर्ण होता गया है। यह केवल पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और यहां तक कि वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करता है। यह लेख जलवायु समझौते की मूल अवधारणाओं, ऐतिहासिक विकास, प्रमुख समझौतों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हम इस विषय को शुरुआती लोगों के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि जटिलताओं को भी संबोधित करेंगे।
जलवायु परिवर्तन की मूल बातें
जलवायु परिवर्तन, जिसे अक्सर वैश्विक ऊष्मीकरण के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस) के जलने से होता है, जो ग्रीनहाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) को वायुमंडल में छोड़ता है।
ये गैसें सूर्य से आने वाली गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे पृथ्वी के वायुमंडल में फंसा लेती हैं, जिससे ग्रह गर्म होता है। इस प्रक्रिया को ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम गंभीर और व्यापक हैं, जिनमें शामिल हैं:
- समुद्र के स्तर में वृद्धि
- अधिक लगातार और गंभीर मौसम की घटनाएं (जैसे तूफान, सूखा, बाढ़)
- जैव विविधता का नुकसान
- कृषि उत्पादकता में कमी
- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल) जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करने वाला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
जलवायु समझौते का विकास
जलवायु परिवर्तन की समस्या को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को 1990 के दशक में मान्यता दी गई थी। जलवायु समझौते का विकास कई चरणों में हुआ है:
- **1992 का रियो समझौता**: यह पहला व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना था। इसने एक सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने में अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है।
- **1997 का क्योटो प्रोटोकॉल**: यह समझौता विकसित देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए, और कई अन्य देशों ने लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष किया।
- **2015 का पेरिस समझौता**: यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस समझौते में सभी देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है। पेरिस समझौता 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य पर भी जोर देता है, जिसका अर्थ है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
पेरिस समझौते की मुख्य विशेषताएं
पेरिस समझौता कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तंत्रों पर आधारित है:
- **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी)**: प्रत्येक देश अपने स्वयं के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिसे एनडीसी के रूप में जाना जाता है।
- **पारदर्शिता**: देशों को अपने उत्सर्जन और प्रगति की नियमित रूप से रिपोर्ट करनी होती है।
- **वैश्विक स्टॉकटेक**: हर पांच साल में, देशों की सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर हैं।
- **जलवायु वित्त**: विकसित देशों को विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान
अभी ट्रेडिंग शुरू करें
IQ Option पर रजिस्टर करें (न्यूनतम जमा $10) Pocket Option में खाता खोलें (न्यूनतम जमा $5)
हमारे समुदाय में शामिल हों
हमारे Telegram चैनल @strategybin से जुड़ें और प्राप्त करें: ✓ दैनिक ट्रेडिंग सिग्नल ✓ विशेष रणनीति विश्लेषण ✓ बाजार की प्रवृत्ति पर अलर्ट ✓ शुरुआती के लिए शिक्षण सामग्री